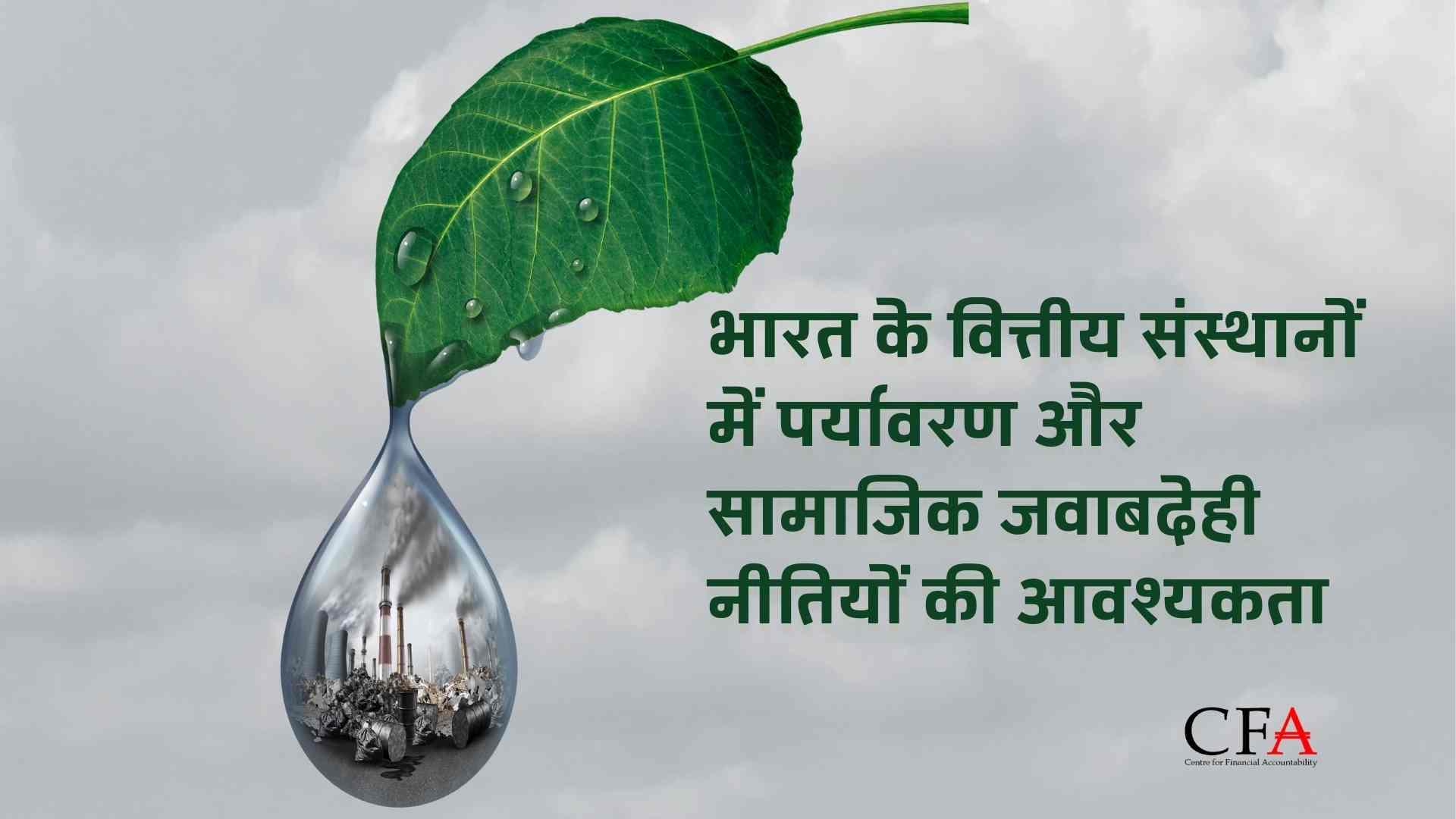ज़्यादातर देशों द्वारा बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य माना जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में भी अधिक मान्य है। वास्तव में वृहद आधारभूत संरचनाएं और विकास परियोजनाएं औपनिवेशिक काल से ही विकास के प्रतिमान का द्योतक रही हैं। बड़े बांध, कोयला एवं अन्य खनिजों की बड़ी खनन परियोजनाओं और भारी उद्योगों ने देश के कथित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1990 के बाद हमारे देश में विकास की अवधारणा में, जनता को लाभ पहुंचाने वाले सामाजिक बुनियादी ढाँचे के बजाय वृहद संरचनाओं की ओर एक तीव्र झुकाव आसानी से देखा जा सकता है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों के इलाकों और प्राकृतिक संसाधनों के बीच परस्पर जुड़ाव बनाते हुए विभिन्न विशालकाय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तथा ऊर्जा सहित अन्य परियोजनाओं का विस्तार, तेजी से जारी है। आर्थिक विकास के विमर्श में इन परियोजनाओं के योगदान को आँका तो जाता रहा है लेकिन परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदाय, जिनका जीवन और आजीविका परियोजना स्थल के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुयी है, पर पड़ने वाले प्रभावों की लगातार अनदेखी की जाती रही है।
ज़्यादातर देशों द्वारा बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य माना जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में भी अधिक मान्य है। वास्तव में वृहद आधारभूत संरचनाएं और विकास परियोजनाएं औपनिवेशिक काल से ही विकास के प्रतिमान का द्योतक रही हैं। बड़े बांध, कोयला एवं अन्य खनिजों की बड़ी खनन परियोजनाओं और भारी उद्योगों ने देश के कथित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1990 के बाद हमारे देश में विकास की अवधारणा में, जनता को लाभ पहुंचाने वाले सामाजिक बुनियादी ढाँचे के बजाय वृहद संरचनाओं की ओर एक तीव्र झुकाव आसानी से देखा जा सकता है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों के इलाकों और प्राकृतिक संसाधनों के बीच परस्पर जुड़ाव बनाते हुए विभिन्न विशालकाय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तथा ऊर्जा सहित अन्य परियोजनाओं का विस्तार, तेजी से जारी है। आर्थिक विकास के विमर्श में इन परियोजनाओं के योगदान को आँका तो जाता रहा है लेकिन परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदाय, जिनका जीवन और आजीविका परियोजना स्थल के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुयी है, पर पड़ने वाले प्रभावों की लगातार अनदेखी की जाती रही है।
जहां एक ओर विकास परियोजनाओं की संख्या में इजाफ़ा हुआ है वहीं इन परियोजनाओं के दुष्प्रभावों के खिलाफ़ लामबंदी भी हुई है। 1920 में टाटा द्वारा मुलशी पेटा में बनाये जा रहे एक बांध के निर्माण के दौरान जबरिया विस्थापन के खिलाफ़ पुणे में 11,000 से अधिक लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया था जो केवल एक शुरुआत थी। 1930 में पहले कंक्रीट बांध के निर्माण के बाद देश में प्रमुख बांधों की संख्या 1950 तक बढ़कर 100 तथा 1985 तक 1000 से अधिक हो गई थी। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, भारत में 2022 तक 5,265 बड़े बांध बन चुके हैं तथा 437 निर्माणाधीन हैं। इस संदर्भ में सीडब्ल्यूसी द्वारा 54 बड़े बांधों के महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चलता है कि एक बड़े बांध से विस्थापित होने वाले लोगों की औसत संख्या 44,182 होती है। देश में बांधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन उनसे बड़े पैमाने पर हो रहे विस्थापन और अन्य मुद्दों को हल करने के तंत्र विकसित नहीं किए गए हैं। डाउन टू अर्थ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नियोजित विकास के पहले तीन दशकों के भीतर विस्थापित लोगों में से केवल पच्चीस प्रतिशत लोगों का ही पुनर्वास किया गया है। भाखड़ा-नंगल परियोजना (1960) के दौरान ऊना और बिलासपुर जिलों में विस्थापित हुए 2108 परिवारों में से अब तक केवल 750 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया है। अन्य परियोजनाओं की कहानी भी समान ही है। सरदार सरोवर परियोजना एक व्यापक रूप से जानी जाने वाली परियोजना है। इसमें 3,000 छोटे, 135 मध्यम और 30 बड़े बांध एवं नहर परियोजनाएं शामिल हैं जो 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा घाटी में बनाए जाने के लिए योजनाबद्ध हैं। प्रथम प्रधान मंत्री जवारलाल नेहरू द्वारा परिकल्पित इस बांध के निर्माण का कार्य 1980 के दशक में शुरू हुआ। सरदार सरोवर बांध, उन सभी नियोजित बांधों में सबसे बड़ा बांध है जिसका लोकार्पण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में किया गया था। बांध का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पिछले तीन दशकों से नर्मदा घाटी के लोगों ने विस्थापन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है। इतने लंबे संघर्ष के बाबजूद घाटी में करीब 200 गांव डूब के कगार पर अभी भी खड़े हैं। हजारों लोग अब भी मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।
द्रुत गति से बढ़ रही कथित विकास परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन का समाधान निकालने के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। तेज़ी से बढ़ते विस्थापन की सबसे अधिक मार देश के आदिवासी समुदाय पर पड़ रही हैं। 2016 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गयी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1950 से 1990 के बीच देश में 87 लाख आदिवासी विस्थापित हुए थे जो कुल विस्थापितों का 40 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे आदिवासी बहुल राज्य, भारत के कोयला भंडार का 70 प्रतिशत, उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का 80 प्रतिशत, बॉक्साइट का 60 प्रतिशत और क्रोमाइट भंडार का लगभग लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, इसलिए ये खनिज दोहन एवं खनन परियोजनाओं का केंद्र बन गए हैं। साफ जाहिर है कि यदि विकास के प्रतिमान का सही तरीके से आकलन नहीं किया गया तो इसकी मानवीय क्षति भयावह हो सकती है। आंतरिक विस्थापितों की निगरानी रखने वाले केंद्र (आईडीएमसी, 2007) के अनुसार, कथित विकास प्रेरित परियोजनाओं के चलते 21.3 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ है जिसमें बांधों से 16.4 मिलियन, खानों से 2.55 मिलियन, औद्योगिक विकास से 1.25 मिलियन और वन्यजीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों से 0.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।
विस्थापन, त्रासदी के विभिन्न पहलुओं में से एक है। परियोजनाओं का पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव चिंता का एक और गंभीर विषय है जिसे अब तक उस गंभीरता से नहीं लिया गया है जितना यह महत्वपूर्ण था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (2020) के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए देशों में 5वें स्थान पर हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करते हुए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी, 2021) कहना है कि भारत में जलवायु संकट के अधिकांश प्रभाव अपरिवर्तनीय हैं, जिन्हें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी लाने की बावजूद सुधारा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत के वित्तीय संस्थान पिछले वर्षों की तरह, छह देशों में से तीसरे सबसे बड़े निवेशक थे जो दुनिया के कोयला निवेश का 80 प्रतिशत वित्तपोषण करते थे। सागरमाला, समुद्री अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एक बंदरगाह आधारित विकासात्मक परियोजना है, जिसमें 6.01 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 574 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में 121 पूरी हो चुकी हैं तथा 201 विकास के चरण में हैं। इसमें अब तक कुल 7,78,080 करोड़ के निवेश में से 1 प्रतिशत से भी कम राशि सामुदायिक विकास के लिए खर्च की गई है। पारिस्थितिकीय तंत्र को होने वाले संभावित नुकसान की रोकथाम अथवा उसकी तैयारी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। भारतीय तट घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां मछुवारा समुदायों के 40 लाख लोगों की अनुमानित आबादी हैं। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने चक्रवात, तूफान, ज्वार-भाटे की आवृत्ति में वृद्धि की है। क्षेत्र में इन घटनाओं की बारंबारता, बड़े पैमाने पर तटीय कटाव सहित अन्य पर्यावरणीय प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहे है। केरल में शनगुमुघम और कोवलम समुद्र तट के अनियमित तटीय कटाव इसी प्रकार के उदाहरण हैं जो विझिंजम समुद्री बंदरगाह के टूटने के कारण हो सकते हैं।
मौजूदा विकास की अवधारणा में, विभिन्न परियोजनाएँ अलग-थलग ना होकर व्यापक रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 2000 के दशक में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की शुरुआत हुयी थी जिसमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। गहराई से पड़ताल करने पर ज्ञात होता है कि ये सभी विशेष आर्थिक क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। आज विकास का मॉडल एक इंटरलॉक सिस्टम बन गया है जो एक दूसरे से गूँथा हुआ है। इसलिए अब यह परियोजनाएं नहीं, बल्कि परियोजनाओं का एक समूह है जैसे – स्मार्ट सिटी, सागरमाला, भारतमाला, औद्योगिक गलियारे, सड़क और रेल गलियारे, सौर ऊर्जा पार्क, थर्मल पावर क्लस्टर आदि। विशालकाय परियोजनाओं के ये समूह, पारिस्थितिकी और सामाजिक क्षति के साथ-साथ भारी वित्तीय लागत का आधार बन गए हैं।
नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अभी अकेले कुल 7,400 परियोजनाएँ हैं। जिनमें से 2020 तक 1.10 लाख करोड़ रुपए (US$ 15.09 बिलियन) लागत वाली 217 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी है। इसी तरह गति शक्ति मास्टर प्लान में 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 100 कार्गो टर्मिनल, 11 औद्योगिक गलियारे, रक्षा उत्पादन में 1.7 लाख करोड़ रुपये का कारोबार, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 109 फार्मास्युटिकल क्लस्टर के अनुबंध शामिल हैं। इसके तहत राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाना है। सिर्फ इस योजना के भीतर ही 5590 किलोमीटर सड़क, 17000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बनाया जाना है।
गति शक्ति योजना अपने आप में एक विशाल मिशन की तरह है। जबकि यह विभिन्न गति शक्ति योजना एक विशाल मिशन की तरह लग सकती है, लेकिन यह कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इसके अलावा कम से कम 20 अन्य मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनमें बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप प्रोजेक्ट, कम से कम 25 शहरों में मेट्रो रेल, कल्पसर बांध परियोजना, गुड्स एंड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भारतमाला परियोजना (इसके तहत देश के 550 जिलों को आपस में जोड़ने वाला 26000 किमी का आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाना है जिसकी अनुमानित लागत 6,92,324 करोड़ रुपये है), कम से कम सात अल्ट्रा-मेगा बिजली परियोजनाएं (प्रत्येक की अनुमानित लागत 15000 करोड़) का लक्ष्य है। 25 सोलर पार्क (अल्ट्रा-मेगा सौर परियोजना) जिन्हे 2017 में बढ़ाकर 50 कर दिया गया था को बनाया जाना लक्षित है जिसमें कई सोलर पार्कों का काम पूरा हो चुका हैं कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं। यहाँ मुख्य सवाल यह उठता है कि इन विशालकाय परियोजनाओं का वित्तपोषण आखिरकार कौन कर रहा है?
पुस्तिका यहां पढ़ें और डाउनलोड करें: भारत के वित्तीय संस्थानों में पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता
Read this in English here.